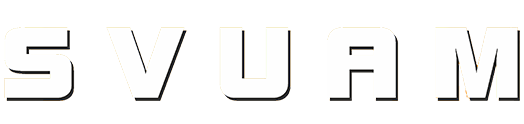सन्तों का इस धराधाम पर आगमन लोक कल्याण के लिए होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय होता है। जीवन का परम लक्ष्य – ‘परमानन्द की प्राप्ति तथा दुःखों की अत्यांतिक निवृत्ति तथा इस के ज्ञान का प्रसार तथा अज्ञान की समाप्ति’- उनकी प्रत्येक क्रिया इस प्रयोजन से होती है। जिस प्रकार गुड़ की डली में हर तरफ़ मिठास ही मिठास भरी रहती है तथा मिठास के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उसी प्रकार शिरोमणि स्वामी विचारानन्द जी की प्रत्येक क्रिया का एक मात्र प्रयोजन अज्ञान-अंधकार की निवृत्ति है तथा इस के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है।
admin
12 April 2017
No Comments
सम्पादक की ओर से
सन्यास से पूर्व हम लोग एक साल में स्वामी जी के तीन जन्मदिन मनाते थे। पहला विक्रमी संवत् के हिसाब से उनका जन्मदिन अर्थात अहोई अष्टमी। दूसरा अंग्रेजी हिसाब से बाईस अक्टूबर तथा तीसरा उनकी रिकार्ड की जन्म तिथि अर्थात चार अप्रैल को। इन तीनों उत्सवों का उद्देश्य – वही ज्ञान चर्चा ही रहता था।
संन्यास धारण के पश्चात इनका एक ही जन्मोत्सव -अर्थात अहोई अष्टमी को मनाया जाता है। भक्त लोग उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। इसी अवसर के लिए इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। जो भक्तों के लिए स्थाई प्रसाद का काम करेगी।
प्रस्तुत पुस्तिका स्वामी जी द्वारा भक्तों को समय – समय पर लिखे गए पत्रों का संग्रह है। यह पत्र पात्रानुसार कथा रूप में लिखे गए हैं। इनका प्रकाशन श्री दयाराम जी फ़ोरमेन के सहयोग से सम्भव हुआ है। आशा है भक्तों के कल्याण में यह पुस्तिका सहायक होगी।
विचार प्रसाद
अपने निकास, विकास, विनाश के अधिष्ठान को लक्षित करने का वाणी अमरवाणी कहलाती है। भेद ग्रंथियों को नष्ट करने वाली लिनि अमरवाणी सद्ग्रंथ कहलाती है। सद्ग्रंथ के अनुगामी को पन्थी तथा पथियों के समूह को पन्थ कहा जाता है। ‘अमरवाणी’ ग्रंथ तथा पंथ का जीता जागता आदर्श रूप संत कहलाता है। स्वयं संत ही वाणी रूप होकर ग्रंथ तथा पंथ का रुप धारण करता है। संत ही निज मत अनुगामियों को क्लेश, कर्म तथा कर्मफल संस्कारों से मुक्ति प्रदान करता है। ऐसे ज्ञान स्वरुप संत को अवतरित हुए चिरकाल व्यतीत हो गया है। इसी से जीव अज्ञान के कारण भ्रमित हो क्लेश कर्म आदि में फंसता जा रहा है। ऐसे में जीव, संत स्वरुप लिखित वाणी मय ग्रंथ के अनुगामी बनें तो निश्चय ही अज्ञान से छुटकारा ले सकते हैं।
साधु श्री निश्चलदास जी के शब्दों में :
जेती बानी बैखरी, ताको अलम पिछान ।
हेतु मुक्ति को ज्ञान लखि, अद्वै निश्चय ज्ञान ।।
समस्त भाषाओं में संत प्रतिपादित ग्रंथों का सारमय प्रयोजन अज्ञान से छुटकारा पाना है। अज्ञान से छुटकारा ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान अद्वितीय जानकारी को कहते हैं। जड़ चेतन को ‘एक मानना’ भूल है, ‘अज्ञान’ है, ‘जीवत्व’ है। देह ‘नश्वर है यह जड़ देह पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहती। यह तो केवल बीच के काल में ही भासती है। जैसे मृगतृष्णा का जल पहले भी नहीं था। जानने के पश्चात भी नहीं रहता चाहे दीखता भी रहे। ऐसे ही यह मृगतृष्णावत भासती है। यह मिथ्या मात्र है। केवल दृष्टि काल में ही भासती है। देह के विकार- ‘जन्म, अस्ति, वृद्वि, क्षय तथा नाश आदि’ देह को देखने वाले द्रष्टा या जानने वाले ज्ञाता में नहीं होते। यह द्रष्टा-ज्ञाता तो असंग ही रहता है। देहादि जगत का तो नाश हो जाता है परन्तु इनके नाश को जानने वाला ज्ञाता अविनाशी ही रहता है। देहादि तो विकार को प्राप्त होते है। पर यह ज्ञाता निर्विकार रहता है। देहादि आकार नाश को प्राप्त होते हैं। पर ज्ञाता निराकार होने से अजर अमर रहता है। निराकार ज्ञाता बहुत से तो हो नहीं सकते। अतः यह ज्ञाता ही सर्वस्व है। मैं भी, तू भी, सर्व भी। सब ज्ञाता-ज्ञाता एक ही है।
हम तेरी चाह में ए यार वहीं तक पहुंचे।
होश ये भी न जहां हैं कि कहां तक पहुंचे।।
अर्थात् ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति । केवल इस सवज्ञाता को विशेषणों से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है । जानने वाले को कैसे जाना जाए?
‘विज्ञाता केन विजानियात’। (वृहदारण्यक उपनिषद)
इसी ज्ञाता को द्रष्टा, असंग, अविनाशी, निर्विकार, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वस्व, मैं, तू, सत्-चित्-आनंद, घन आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसा सद्सत सद्ग्रंथ प्रतिपादित करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे संतों या ग्रंथों को मनु रुप (शरीर रुप) आकार रुप देखते हैं। वे भ्रमित है, अज्ञानी है। ये अज्ञानी जैसे स्वयं को देह रुप देखते हैं। वैसे ही सन्त तथा ग्रंथ को भी देह रुप ही देखते हैं। ये ‘देहधारी’ अन्धे ही हैं। इनके पास ‘ज्ञानदृष्टि’ का नितांत अभाव है। इसीलिए इस संसार में भी महादुःखी रहते हैं। तथा पानी में जाकर भी यमराज की यातनाएं सहते हैं।
सन्त मनुष कर जानते, ते नर कहिए अंध ।
महादुःखी संसार में, आगे जम को फंद।।
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं- ‘हे अर्जुन । मूढ़ लोग मनुष्य के अधिष्ठान स्वरुप परम अविनाशी को नहीं जानते जिसमें सर्वभूत भासते हैं।
अवजानंति मां मूढा मानू तनुमश्रितम् ।
परमभावं मां न जानंति, ममभूत महेश्वरम।।११।६
ऐसे ही ग्रंथ के प्रयोजन रुप चित्-जड़ ग्रंथि भेदन को समझकर ग्रंथ पूजा, ग्रंथ पाठ में लगे रहते हैं।
कहा ग्रंथ गण के पढ़े, किन कर्मो के कीन।
चित्त-जड़ ग्रंथि प्रबोधिनी, धी जब उर प्रगटीन ।।
हम समय-समय पर जो पत्र जिज्ञासुओं को लिखते रहे हैं, उनमें से कुछ पत्रों को श्री घनश्याम शर्मा ने संग्रहित करने का प्रयास किया है। इन पत्रों में चित्- जड़- ग्रंथि – विवेक विषय पर लिखे गए पत्रों को चुनकर ‘प्रसादम्’ पुस्तक का रुप दिया गया है ।विषय को श्रृंखलाबद्व रखना, मूल साधुक्कड़ी भाषा को न छोड़ना, चित्- जड़ग्रंथि भेदन रुपी प्रयोजन को स्पष्ट करना इस ग्रंथ की विशेषता है ।शर्मा जी ने अपने विवेक से स्वल्प अक्षरों को सहज, सरल, सरस शब्दों में तथा सारगर्भित वाक्यों में अमर सदेंश स्वरुप ‘प्रसादम्’ पुस्तक भेंट की है। निश्चय ही पाठक वृंद इस ‘प्रसादम्’ को ग्रहण कर कृतकृत्य हो जाएंगे।
कुछ ऐसा अपनी आंखों में, बस जाता है नूरे हुस्ने अजल।
हर वक्त निगाहों में यकसां, एक मोहिनी मूरत रहती है।
तृतीय संस्करण
तत्वमसि
(प्रसादम्)
स्वामी विचारानन्द जी महाराज से कृपा प्रसाद स्वरुप प्राप्त तत्वमसि प्रसादम् का तृतीय संस्करण प्रस्तुत करने का सुअवसर मिलने पर कृतार्थ हूं । प्रस्तुत पुस्तिका स्वामी जी द्वारा भक्तों को समय – समय पर लिखे गए पत्रों का संग्रह है। यह पत्र पात्रानुसार कथा रूप में लिखे गए हैं।
प्रथम और द्वितीय संस्करण की सफ़लता जिज्ञासु जनमानस के ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य की सफलता को दर्शाता है। ज्ञान की ओर अग्रसर मुमुक्षु जनों की तृषा को सोलह पत्रों की सोलह कहानियों के माध्यम से परिपूरित करती है और अंधकार से प्रकाश की ओर के मार्ग पर अग्रसर हो ‘अद्वै निश्चय ज्ञान’ जैसे सिद्धान्तों से पूरित करती है।
मुमुक्षु जनों की मांग पर, स्वामी विचारानन्द जी वेदान्त वागीश (श्री कामाख्या मन्दिर, तपो भूमि आश्रम, परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश) का आशीष से, तथा श्री दीपक कोचर जी, (कानपुर वाले) के सहयोग १३स पुस्तिका का तृतीय संस्करण प्रस्तुत है। पिछले संस्करणों की त्रुटियों को इस संस्करण में दूर करने का प्रयास किया गया है।
आशा है भक्तों के कल्याण में यह पुस्तिका सहायक होगी। पुस्तिका को और लाभकारी बनाने हेतु, दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत है।
मुमुक्षु जनों की सेवा में,
विपिन चन्द्र ‘ज्योतिर्मय’
Copyright © 2025 Svuam.org